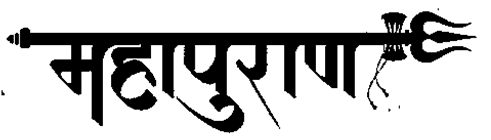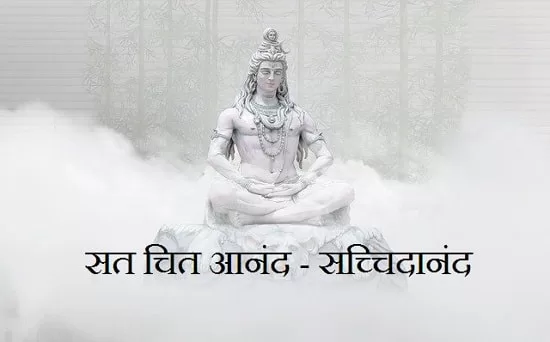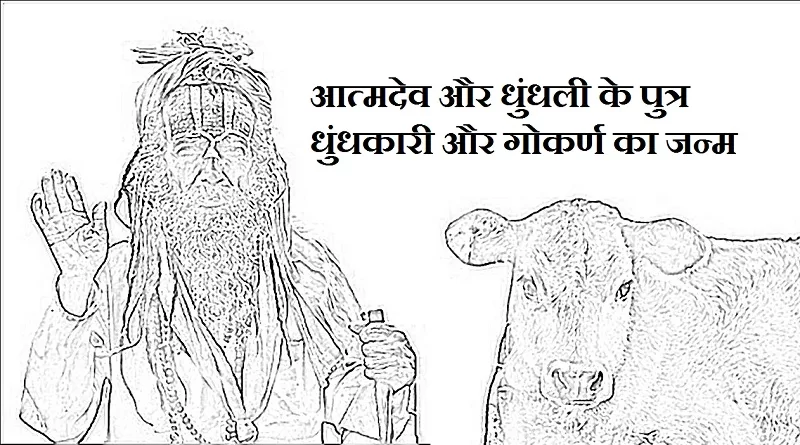परमात्मा अर्थात परम आत्मा को ही सत चित आनंद (Sat Chit Aanad in Hindi) कहा जाता है। परमात्मा ही सच्चिदानंद है। यहाँ हम सच्चिदानंद का संक्षिप्त में अर्थ और एक कहानी से समझने की कोशिश करेंगे।
सत चित आनंद का अर्थ Sat Chit Anand meaning –
सत – अर्थात सत्य (True) – वेदपुराणो के अध्ययन से सत्य को खोजना
चित – अर्थात चेतना (consciousness) – मन की जागृत अवस्था / सत्य से परिचित जीव
आनंद – सुखी (pure happiness) – जीव या व्यक्ति को सत्य का पता चलने के बाद सम्पूर्ण आनंद (pure happiness) की अनुभूति प्राप्त होती है।
इसलिए सत + चित + आनंद को मिलाकर शब्द बना है सच्चिदानंद।
इसलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है क्युकी परमात्मा ही सम्पूर्ण सत्य है, सम्पूर्ण चेतना है, और सम्पूर्ण सुख है। केवल मनुष्य ही इस सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकता है अन्य जीव नहीं ।
अब सच्चिदानंद से के रहस्य को समझाने वाली एक कहानी पढ़ते है –
सुखी कौन है ? (Sat Chit Aanad in Hindi – Pauranik katha)
उत्तम प्रदेश (उत्तराखंड) के राजा जिसके राज्य में हर प्रकार की सुख-सुविधाएं थी. लेकिन राजा का मन प्रसन्न नहीं था, वह बीमार सा अनुभव कर रहा था। सारी सुविधाओं के होते हुए भी खिन्न था। उसने दरवार में ये चिंता सभी मंत्रियो को बताई की वह सुखी नहीं है। और इस बात का कारण उसे भी नहीं पता।
सभी मंत्रियो ने विचार विमर्श किया और राजगुरु से पूछा।
राजगुरु मुस्कराते हुए बोले – हे राजन ! बस इतनी सी बात। इसका एक रास्ता है मेरे पास। आप बस एक रात के लिए किसी सुखी व्यक्ति की कमीज पहन कर सो जाइये। उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपका जीवन बदल देगी। और आप फिर से सुखी हो जायेगे।
राजा प्रसन्न हो गया। फिर उसने अपने सैनिको को आज्ञा दी – की जाओ अपने राज्य में किसी भी सुखी व्यक्ति की कमीज एक रात के लिए लेकर आ जाओ।
राजा के सैनिक कई महीने तक राज्य में ऐसा व्यक्ति ढूढ़ते रहे, जो स्वयं को सुखी कह सके, लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला. सिपाही भी थक हार कर परेशान हो गए थे, एक वृक्ष के नीच बैठ कर चिंता कर रहे थे की कही खाली हाथ वापस लौटना पड़ा तो दंड मिलेगा।
तभी पास ही दूसरे घने पेड़ के नीचे अपनी बैलगाड़ी के पास विश्राम करते गाड़ीवान के मुंह से उन्होंने सुना, हे ईश्वर ‘जैसा मैं सुखी, वैसा सुख सबको मिले!’
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत।
अर्थ – “सभी सुखी होवें, सभी रोगमुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बनें और किसी को भी दुःख का भागी न बनना पड़े।”
राजा के सैनिक तुरंत उसकी ओर दौड़े और उससे पूछा कि क्या तुम सुखी हो?
गाड़ीवान बोला – हा भाई, क्या में दुखी दीखता हु? में सुखी हु
सैनिक – सच सच बता, क्या आप सुखी है?
गाड़ीवान बोला – देखो भाई ! मेरे बैल चारा खाकर सुस्ता रहे है, वो भी सुखी, में भोजन करके आराम कर रहा तो में भी सुखी। क्या इतना भी नहीं दिखता?
सैनिक – पर तुम्हारे पास तो कमीज भी नहीं है? तुम सुखी कैसे हो सकते हो?
गाड़ीवान बोला – कमीज से सुख मिलता है किसने बोला? में तो वैसे ही सुखी हु. उस गाड़ीवान ने कहा, ‘मेरे सुख को किसी कमीज की जरूरत नहीं’.
तो सैनिकों ने उससे कहा, ‘तुम्हें राजा के पास चलना होगा. राजा ऐसे आदमी की तलाश कर रहे हैं जो सुखी हो’.
गाड़ीवान ने जाने से मना कर दिया. सैनिकों ने तुरंत राजा को जाकर यह बात बताई. राजा ने उसके लिए कई प्रलोभन भेजे, लेकिन उसने आने से इंकार कर दिया और कहा, ‘राजा को जरूरत है तो स्वयं आएं. मुझे राजा की जरूरत नहीं’.
फिर राजा रथ पर सवार होकर मंत्रियो और सैनिको के साथ उससे मिलने पहुंचा, लेकिन उसने राजा से मिलने से इनकार कर दिया.
फिर राजा पैदल अपने मंत्रियो और सैनिको के साथ आया, फिर भी उसने इंकार कर दिया।
तीसरे प्रयास में जब राजा साधारण कपड़ो में अकेला गाड़ीवान से मिलने गया, तो गाड़ीवान ने उससे बात करना स्वीकार किया.
लेकिन तभी गाड़ीवान बोला – राजा क्या मेरी पीठ खुजा सकेगा?
राजा बोला – हा मालिक, और राजा पीठ खुजाने लगा।
गाड़ीवान बोला – रहने दे राजा। अगर पहले ही अपने दिखावा छोड़कर आता तो मेरी पीठ नहीं खुजानी पड़ती।
गाड़ीवान बोला – पूछो राजा! क्या पूछना चाहते हो?
राजा बोला – महाराज ! ये क्या रहस्य है की जिसके पास ढेरो कमीज है वह सुखी नहीं है, लेकिन जिसके पास एक भी कमीज नहीं है वह सुखी है?
गाड़ीवान बोला – मेरे सुख का कारण कमीज नहीं बल्कि सत चित आनंद स्वरुप आत्मा है, जो भी यह जान लेता है की सुख मनुष्य के भीतर है उसे उसे सुख के लिए बाहरी वस्तुओ की आवश्यकता नहीं पड़ती।
राजा – परन्तु मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के ओर भागता रहता है?
गाड़ीवान बोला – राजे! जो व्यक्ति अपने अंदर की सत चित आनंद स्वरुप आत्मा को जान लेता है वह व्यक्ति बाहरी सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता। राजन आत्मा आनंद का रूप है। आत्मा आनंद है तो इसलिए चारो तरफ आनंद ही आनंद है।
आत्मा के आनंद स्वरुप के कारण ही व्यक्ति स्वयं से हर क्षण प्रेम करता है। क्या तुम जानते हो? की जब व्यक्ति बूढा हो जाता है, बीमार हो जाता है। इन्द्रियाँ साथ छोड़ रही होती है, मृत्यु दरवाजा खटखटा रही होती है लेकिन मनुष्य तब भी स्वयं से प्रेम करना नहीं छोड़ता। व्यक्ति तब भी स्वयं से हर क्षण हर पल प्रेम करता है। यदि दुःख आत्मा का स्वरुप होता तो क्या मनुष्य स्वयं से इतना प्रेम करता?, नहीं न।
गाड़ीवान – राजन! तो वही, क्या तुमने कभी सोचा है की मनुष्य के अंदर आत्महत्या का विचार क्यों आता है?
राजा – नहीं मालिक! कृपया आप बताये!
गाड़ीवान – राजन! आत्महत्या का विचार क्या है ? क्यों भावना के वश में आदमी मन, बुध्दि और शरीर आदि को ख़त्म कर देना चाहता है? क्युकी आत्महत्या का विचार भी आत्मप्रेम को ही व्यक्त करता है। जब व्यक्ति दुःख और दुःख देने वाली स्थितियों से छुटकारा नहीं प्राप्त करता तो मनुष्य अज्ञानता में आत्महत्या को ही दुखो से छुटकारा प्राप्त करने का रास्ता समझता है। इतना है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम की वह अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देना चाहता है।
राजा – तो मनुष्य बाहरी संसार की तरफ भागता क्यों है?
गाड़ीवान – क्युकी वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता हो चाहे वो धन हो, वैभव हो, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, वे सब सुख के उपकरण है जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है।
लेकिन मनुष्य स्वयं के सम्बन्धी और रिस्तेदार तक भी छोड़ देता है अगर वे दुःख का कारण बन जाते है। क्युकी वह उन सबमे सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। यहाँ तक की मनुष्य स्वयं से इतना प्रेम करता है की अपने सुख के लिए किसी को भी छोड़ सकता है। स्वयं को समाप्त भी करना पसंद करता है। अर्थात एक तरफ स्वयं का सुख होता है तो दूसरी तरफ पूरा संसार। स्वयं के लिए इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरुप का प्रमाण है।
यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुखो से प्रेम करता । चूँकि हम अज्ञानतावश अपने आनंद स्वरुप को नहीं जानते इसलिए संसार के छोटे मोटे सुखो को प्राप्त करने के लिए ज़िंदगी भर भागते रहते है। ये बिलकुल वैसा ही की जो सुखो का राजा है, जो सुखो का स्वामी है। वह खुद को भिखारी समझ दुसरो के सामने सुख के लिए गिड़गिड़ाता रहता है। यही है अज्ञान की शक्ति।
इसलिए राजन! सम्बन्धो का सुख और वस्तुओं का सुख स्थाई नहीं होता, परन्तु आत्मा का आनंद असीम होता है, यह अनंत है जो कभी ख़त्म नहीं होता।
राजा – आत्मा का आनंद कैसे स्थाई है?
गाड़ीवान – राजे ! जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु को देखते है तो उससे आनंद होता है इस आनंद को शास्त्र-प्रिय कहते है। और जब हम उस व्यक्ति या वस्तु को पा लेते है तो वह आनंद कई गुना बढ़ जाता है तो उसे मोद कहते है। जब हम उस वस्तु या व्यक्ति का उपभोग करते है तो उससे प्राप्त आनंद को प्रमोद कहते है।
परन्तु जैसे ही हम उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग हो जाते है तो वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजन! व्यक्तियों का आनंद, वस्तुओं का आनंद स्थाई नहीं होता, परन्तु आत्मा का आनंद स्थाई और अनंत होता है।
और अंत में राजा ने वह प्रश्न किया जो इस समय हम सबके मन में है।
राजा – यदि में ही आत्मा आनंद हु और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, शरीर, मन, बुद्धि, और बाहर किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है। तो वह अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव मैं क्यों नहीं कर सका?
गाड़ीवान – हे राजन ! जब तक तुम अपनी आँखे बंद करके रखोगे तो अँधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धी, रस, भाव, और विचारो की तरफ ही देखोगे तब तक आप उस अनंत सुख को अनुभव नहीं कर सकोगे। सुख और दुःख दोनों एक ही हैं. जैसे रात-दिन वैसे सुख-दुख. दुख के लिए मन में जगह बनाओ. उसे स्वीकार करो. दुख को स्वीकार करने से वह सुख में बदल जाता है।
इसमें आत्मा की गलती नहीं है, बल्कि हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजन अगर तुम सुख चाहते है तो आत्मा के अंदर झांको। आत्मा ही सच्चा सुख है लेकिन हम पूरा जीवन बाहर सुख की तलाश में लगे रहते है।
Sat Chit Aanad in Hindi –
जबकि हम खुद ही आनंद है, ये भूल जाते है। जिसका सबसे बड़ा कारण हम सत (सत्य) को नहीं जानते तो चित हमारा बाहरी सुख ढूढ़ने में लगा रहता है, और हम सच्चे आनंद से अनभिज्ञ रहते है। जो व्यक्ति सत या इस आत्मा के आनंद के सत्य से परिचित होता है, उसका चित्त भी शांत हो जाता है, और अनंत आनंद को प्राप्त करता है। यही सच्चिदानंद (Sat Chit Aanad in Hindi) होता है।
राजा और गाड़ीवान में इस आत्मा के आनंद और सुख पर लम्बी चर्चा हुई। जिसे वेदांत में आनंद मीमांसा कहते है। जिसमे सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, कामसिक आनंद से लेकर अलग-अलग प्राणियों में अलग-अलग आनंद की अनुभूति के बारे में गाड़ीवान ने राजा को उपदेश दिया है।
मीमांसा दर्शन हिन्दुओं के छः दर्शनों में से एक है। इस शास्त्र काे ‘पूर्वमीमांसा’ और वेदान्त काे ‘उत्तरमीमांसा’ भी कहा जाता है।
Source: – छांदोग्य उपनिषद